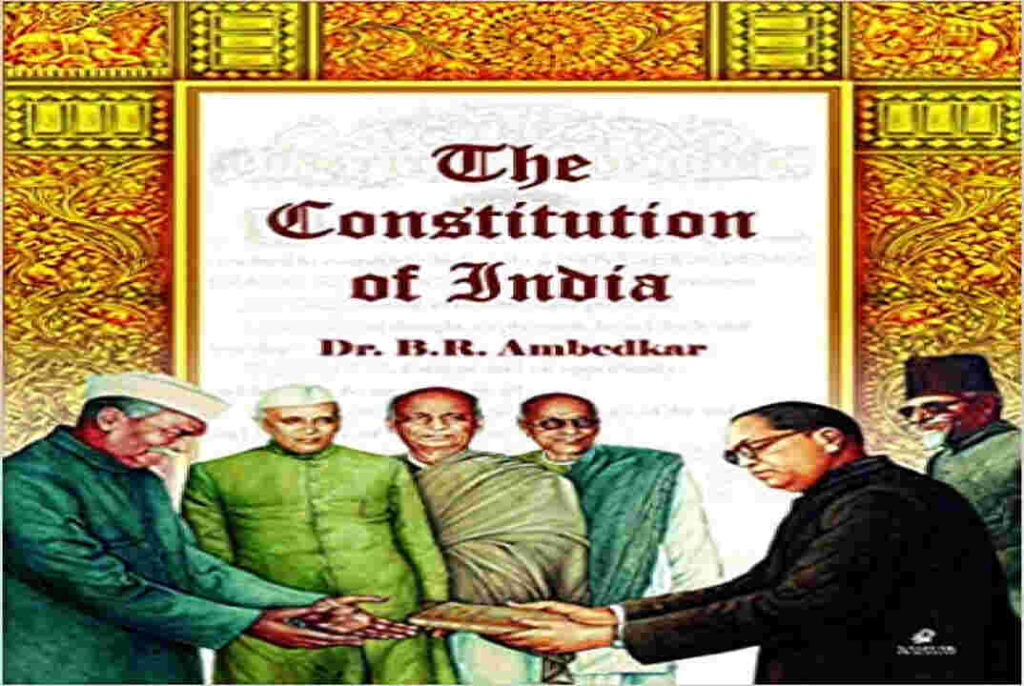
जैसे-जैसे डॉ.बाबासाहेब अंबेडकर भारत के दबे-कुचले लोगों के आत्म-सम्मान और बराबरी वाले भारत की उम्मीद के प्रतीक के तौर पर ऊपर उठ रहे हैं, ब्राह्मणवादी ताकतों और संघ परिवार ने यह दावा और तेज़ कर दिया है कि डॉ. अंबेडकर ने भारतीय संविधान नहीं लिखा था। उनके अनुसार, असली क्रेडिट कानूनी और संवैधानिक एक्सपर्ट बीएन राउ को जाना चाहिए।
यह दावा कितना सच है ? संविधान बनाने में बीएन राउ की क्या भूमिका थी ?
बीएन राउ (1887–1953) मैंगलोर के एक कोंकणी ब्राह्मण थे, जिन्होंने भारत और विदेशों में कानून और संवैधानिक पढ़ाई की बहुत ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार में एक कानूनी एक्सपर्ट के तौर पर काम किया, यहाँ तक कि उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी मिली। उन्होंने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निभाए थे—असम और कश्मीर की रियासतों के प्रधानमंत्री, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज, और संवैधानिक सुधारों पर ब्रिटिश कमेटियों के सदस्य।
उन्होंने कभी भी एंटी-कॉलोनियल संघर्षों या भारत के दबे-कुचले वर्गों के मुक्ति आंदोलनों में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन आज के डेमोक्रेटिक देशों के संविधान और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क पर उनकी ज्ञान की महारत थी।
1946 में, कांग्रेस की अगुवाई वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किया। उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक शुरुआती ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। लेकिन वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे और इसलिए उन्होंने इसकी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ एक एक्सपर्ट के तौर पर सलाह दी।
फरवरी 1947 में, राव ने एक शुरुआती ड्राफ्ट जमा किया। एडवाइजर के तौर पर उनका काम लगभग पूरा हो गया था। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाद में कुछ खास बातों पर उनकी सलाह मांगी, लेकिन फरवरी 1947 के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से डॉ.अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर आ गई।
इसलिए, राऊ का रोल इस प्रोसेस को एक भरोसेमंद शुरुआत देना था, जिसे डॉ.अंबेडकर ने भी माना था। 25 नवंबर, 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने आखिरी भाषण में, डॉ.अंबेडकर ने साफ-साफ कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्रेडिट सिर्फ उन्हें नहीं है। उस क्रेडिट का एक हिस्सा शुरुआती ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बीएन राऊ को, इसे लेजिस्लेटिव फॉर्म में लाने वाले एसएन मुखर्जी को, ड्राफ्टिंग कमेटी को, और कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए भी जाना चाहिए, जिससे मतलब वाली बहस हो सकी।
लेकिन वह एक टेक्निकल और लीगल ड्राफ्ट था। अगर कोई इसकी तुलना फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई बहस से करे, तो कोई डॉ. अंबेडकर की लीडरशिप में असेंबली के लंबे और डेमोक्रेटिक सफर को समझ सकता है, जो राऊ ड्राफ्ट से शुरू हुआ था।
चूंकि डॉ.अंबेडकर ने अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का पद संभाला था और उन्हें अक्टूबर 1947 तक एक बदला हुआ ड्राफ्ट देने का काम सौंपा गया था, जिसमें कई दूसरी कमेटियों की सिफारिशें भी शामिल थीं, इसलिए उन्होंने पहले ही राव के ड्राफ्ट में शुरुआती बदलाव कर दिए थे।
राउ के ‘टेक्निकल’ ड्राफ़्ट से ‘डेमोक्रेटिक संविधान’ तक
फरवरी 1947 और अगस्त 1947 के बीच, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अलग-अलग कमेटियों ने राऊ ड्राफ्ट में बदलाव किए। इस बीच, बंटवारे की वजह से, जिस चुनाव क्षेत्र से डॉ. अंबेडकर चुने गए थे, वह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और उन्होंने अपनी असेंबली की मेंबरशिप खो दी।
लेकिन डॉ.अंबेडकर ने 1919 साउथबोरो कमेटी, 1928 साइमन कमीशन, 1930-32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में अपनी बातों, दलीलों और दखल के ज़रिए गैर-लोकतांत्रिक भारतीय समाज के बारे में गहरी समझ रखने वाले एक महान कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर के तौर पर अपनी पहचान पहले ही बना ली थी। उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी और भारत की सामाजिक बीमारियों की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति के तौर पर पहचाना जाता था। आखिरी वायसराय माउंटबेटन और प्राइम मिनिस्टर एटली जैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर भी डॉ.अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बने रहने के पक्ष में थे।
कांग्रेस ने – अपने विरोधियों को शामिल करने और यह पक्का करने के लिए कि दबे-कुचले लोग नए देश और उसके संविधान पर अपना दावा कर सकें, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत – डॉ.अंबेडकर को बॉम्बे प्रोविंस से फिर से चुनवाया और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया।
जैसा कि स्कॉलर-एक्टिविस्ट आनंद तेलतुंबड़े ने आइकोनोक्लास्ट: ए रिफ्लेक्टिव बायोग्राफी ऑफ़ डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर में बताया है, कांग्रेस के डॉ.अंबेडकर को चुनने के पीछे पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक दोनों कारण थे। अगस्त 1947 तक, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, डॉ.अंबेडकर के सामने यह काम था:
“कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राव के ड्राफ्ट को बदलना और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार करना।”
डॉ. अंबेडकर ने अक्टूबर 1947 तक पूरी तरह से बदला हुआ पहला ड्राफ्ट पूरा कर लिया। नवंबर 1947 से फरवरी 1948 तक, सबकमेटियों ने इस पर बहस की और दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया। फरवरी 1948 से, जनता से आठ महीने तक सुझाव मांगे गए। इन्हें शामिल करते हुए, नवंबर 1948 में, ड्राफ्टिंग कमिटी ने—हालांकि इसमें सात सदस्य थे—फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया, जो असल में डॉ. अंबेडकर की अपनी मेहनत से हुआ था।
नवंबर 1948 से 25 नवंबर 1949 तक, असेंबली ने फ़ाइनल ड्राफ़्ट के हर क्लॉज़ पर बहस की, और आखिर में उसे अपना लिया। इस तरह, राव ने एक ज़रूरी टेक्निकल ड्राफ़्ट दिया। लेकिन इसमें एक डेमोक्रेटिक आत्मा – एक असली भारतीय डेमोक्रेसी – भरने का काम अंबेडकर ने किया।
जब हम राव के ड्राफ़्ट की तुलना फ़ाइनल संविधान से करते हैं तो फ़र्क और साफ़ हो जाता है।
अंतर
1. फंडामेंटल राइट्स: राउ के ड्राफ्ट में फंडामेंटल राइट्स के कोई लागू करने लायक क्लॉज़ नहीं थे। उससे पहले, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, 1946 को ऑब्जेक्टिव्स रेज़ोल्यूशन पेश किया था, जिसमें राइट्स का फ्रेमवर्क दिया गया था, लेकिन डॉ.अंबेडकर ने उन राइट्स और रेमेडीज़ की सुरक्षा की कमी का ज़रूरी सवाल उठाया था।
दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉ. अंबेडकर का पहला भाषण लागू करने लायक राइट्स के लिए था। उनकी लगातार वकालत की वजह से, राइट्स की ज्यूडिशियल सुरक्षा की गारंटी देने वाले आर्टिकल 32 और 226 को शामिल किया गया।
2. सोशल जस्टिस: राउ के ड्राफ्ट में सोशल जस्टिस या बराबरी पर बहुत कम ज़ोर दिया गया था। राउ ड्राफ्ट में सोशल और एजुकेशनल पिछड़ेपन और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ पर फोकस नहीं किया गया था, जैसा कि फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 46 में बताया गया है। राउ के फंडामेंटल राइट्स क्लॉज़ में सोशल जस्टिस पर बस एक छोटी सी बात थी। राउ के ड्राफ्ट में अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्लॉज़ में सोशल स्ट्रक्चर की वजह से बनी असमानता पर ज़ोर नहीं दिया गया था।
फ़ाइनल संविधान में, आर्टिकल 39 (b) और (c) में इसका खास ज़िक्र है।
डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में, छुआछूत खत्म करने (आर्टिकल 17), बराबरी के नियमों को बढ़ाने (आर्टिकल 15 और 16), और इंसानी इज़्ज़त को शामिल करने वाले नियम शामिल किए गए।
3. राज्य की नीति के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स: राऊ के ड्राफ़्ट में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक ही हेडिंग में रखा गया था, जिसमें किसी पर भी ज़ोर नहीं दिया गया था। फ़ाइनल संविधान में, उन्हें दो अलग-अलग चैप्टर्स में बांटा गया था, जिनकी डिटेल में जानकारी दी गई थी। डॉ.अंबेडकर का विज़न—हालांकि वह चाहते थे कि ये फंडामेंटल राइट्स हों—यह पक्का करता था कि उन्हें पार्ट IV के तौर पर जोड़ा जाए ताकि राज्य को सामाजिक और आर्थिक बराबरी की ओर ले जाया जा सके।
4. डेमोक्रेटिक एथिक और प्रस्तावना: राऊ का ड्राफ़्ट सरकार के लिए एक टेक्निकल मैनुअल था। राऊ की प्रस्तावना में सिर्फ़ इतना कहा गया था: “हम, भारत के लोग, सबकी भलाई को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के ज़रिए, इस संविधान को लागू करते हैं, अपनाते हैं और खुद को देते हैं।”
राऊ के लिए, सबकी भलाई ही सब कुछ थी। लेकिन डॉ. अंबेडकर के लिखे आखिरी संविधान के प्रस्तावना में बराबरी और सामाजिक न्याय, और खासकर भाईचारे पर ज़ोर दिया गया था, जिसके बारे में राऊ के ड्राफ़्ट में कोई ज़ोर या खास ज़िक्र नहीं है। अंबेडकर ने, प्रोग्रेसिव सदस्यों के साथ मिलकर, इसे एक नैतिक संविधान में बदल दिया, जिसमें आज़ादी, बराबरी और भाईचारे वाले देश के लिए बदलाव लाने की क्षमता थी।
5. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी
राउ ने सिर्फ़ एक छोटा-सा फ्रेमवर्क दिया, जो मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन और पावर बाउंड्री पर फोकस था, जो असल में गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। डॉ. अंबेडकर और असेंबली ने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल रिलेशन, इमरजेंसी पावर, और भी बहुत कुछ पर डिटेल्ड प्रोविज़न के साथ इसे और बेहतर बनाया। हालात को देखते हुए, भारत ने एक यूनियन-ओरिएंटेड फेडरेशन अपनाया।
6. साइज़
राउ के ड्राफ़्ट में लगभग 240 आर्टिकल थे। अंबेडकर के तहत फ़ाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, जिससे यह एक पूरा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। जबकि राउ का काम एक टेक्निकल कंट्रीब्यूशन था, डॉ.अंबेडकर की लीडरशिप ने एक सेक्युलर, सोशलिस्ट-ओरिएंटेड, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन रिपब्लिक बनाया।
डॉ. अंबेडकर की बेमिसाल मेहनत
26 नवंबर, 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ़ाइनल सेशन में, मौजूद 285 मेंबर्स में से 284 ने अंबेडकर के रोल की दिल से तारीफ़ की। ड्राफ़्टिंग कमेटी के मेंबर टीटी कृष्णमाचारी ने इमोशनल होकर बताया कि डॉ. अंबेडकर के बिना यह काम कितना मुश्किल होता। एक सदस्य की मौत हो गई थी। दो सदस्य इतनी दूर रहते थे कि किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते थे। एक अमेरिका चला गया। दूसरा बीमार था। कृष्णमाचारी खुद एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में लगे हुए थे।
पूरा बोझ डॉ. अंबेडकर पर आ गया, जिन्होंने गंभीर बीमारी के बावजूद, ड्राफ्ट पूरा करने के लिए दिन में 18 घंटे काम किया। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू और दूसरों ने इन बातों का समर्थन किया और देश का आभार व्यक्त किया।
डॉ. अंबेडकर का संविधान ?
यह सब इतिहास में दर्ज है। फिर भी मनुवादी चिल्लाते रहते हैं कि अंबेडकर ने ड्राफ्ट नहीं लिखा या अकेले नहीं लिखा। वही ताकतें यह भी दावा करती हैं कि भारतीय संविधान मनुस्मृति के अलावा कुछ नहीं है।
यह तर्क अपने आप में बेईमानी है। किसी भी डेमोक्रेसी में, कोई भी संविधान एक आदमी नहीं लिखता। इसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद सभी सामाजिक ताकतों की मिली-जुली सोच-विचार से बनाया जाता है। जिन समाजों में दबे-कुचले लोगों के पास पॉलिटिकल ताकत होती है, वहां डेमोक्रेसी ज़्यादा बराबरी वाली बन जाती है। जहां वे कमज़ोर होते हैं, वहां डेमोक्रेसी ताकतवर लोगों का ज़रिया बन जाती है।
अगर अकेले डॉ. अंबेडकर के पास संविधान लिखने की ताकत होती, तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर उन्हें पूरी आज़ादी होती, तो उनके सभी आदर्श – सॉवरेन सोशलिज़्म, बौद्ध बराबरी वाला – फंडामेंटल राइट्स के तौर पर शामिल हो जाते। लेकिन भारत में पूरी तरह अंबेडकरवादी संविधान के लिए ज़रूरी सामाजिक क्रांति नहीं हुई थी।
इस तरह, डॉ. अंबेडकर का उतना ही हिस्सा संविधान में आ सका, जितने हालात इजाज़त देते थे। सच्चे क्रांतिकारी डॉ. अंबेडकर अभी भी इससे बाहर हैं। क्योंकि सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर उनके रेडिकल विचारों को नहीं अपनाया गया, इसलिए आज ब्राह्मणवादी हिंदुत्व और शिकारी कॉर्पोरेट कैपिटलिज़्म मौजूदा संविधान को भी खत्म करने में कामयाब हो गए हैं।
क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार थी?
सिर्फ़ इसलिए कि अलग-अलग ग्रुप एंटी-कॉलोनियल आज़ादी की लड़ाई में एक साथ आए थे, न तो भारतीय समाज और न ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़्यादातर सदस्य ऐसे नागरिक बने जो सच में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ-साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मानते थे। अगर आज भी भारत डॉ. अंबेडकर के बुद्धिस्ट सिविलिटी और प्रबुद्ध सोशलिज़्म के विज़न के लिए तैयार नहीं है, तो तब वह कितना तैयार हो सकता था?
इसलिए, यह दावा कि डॉ. अंबेडकर ने “अकेले ही” कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उतना ही सच है जितना यह दावा कि उनकी कई रेडिकल इच्छाओं को उस समय की हावी पॉलिटिकल-सोशल ताकतों ने जानबूझकर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रखा था।
डॉ. अंबेडकर या किसी दूसरे सदस्य द्वारा रखे गए किसी भी प्रपोज़ल पर पहले संबंधित सब-कमेटी में चर्चा की जाएगी। उसकी मंज़ूरी मिलने के बाद ही वह पूरी असेंबली के सामने आएगा। अगर आम सहमति नहीं बनती, तो ज़्यादातर वोटों के आधार पर प्रपोज़ल या तो स्वीकार कर लिए जाते थे, खारिज कर दिए जाते थे, या उनमें बदलाव किए जाते थे।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने लगभग 7,500 अमेंडमेंट पेश किए, जिनमें से सिर्फ़ 2,500 पर ही असल में बहस हुई।
इस पूरे प्रोसेस में, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, डॉ. अंबेडकर ने अपनी बहुत ज़्यादा जानकारी और दबे-कुचले लोगों के लिए गहरी चिंता का इस्तेमाल करके, अलग-अलग बदलावों को मानने या न मानने के संवैधानिक और राजनीतिक नतीजों पर सदस्यों के साथ शांति से और एनालिटिकल तरीके से बात की। कुछ दूसरी प्रोग्रेसिव ताकतों ने कभी-कभी उनकी कोशिशों का साथ दिया। फिर भी असेंबली ने कई ऐसे बदलावों को नकार दिया जो इस देश को और ज़्यादा इंसानी बना सकते थे, और इसने कई ऐसे बदलावों को भी स्वीकार किया जिन्होंने हमारी आज की गिरावट के बीज बोए।
इसलिए, जब तक हम असेंबली के क्लास-कास्ट बैकग्राउंड और इसके ज़्यादातर सदस्यों के सोच के झुकाव को नहीं समझते, हम सही मायने में उस दिमागी और राजनीतिक मेहनत को नहीं समझ सकते जो अंबेडकर ने संविधान को जितना हो सके दबे-कुचले लोगों के हक में बनाने के लिए की थी।
संविधान सभा कितनी रिप्रेजेंटेटिव थी?
पूना पैक्ट के बाद, डॉ. अंबेडकर इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि अगर भारत को ऊंची जाति के हिंदुओं के दबदबे में आज़ादी मिली तो दलितों और दूसरे दबे-कुचले ग्रुप्स के अधिकारों का क्या होगा। उन्होंने एक ऐसी संविधान सभा की ज़रूरत पर भी सवाल उठाया जिसमें ज़्यादातर सवर्ण और एलीट लोग होंगे।
उन्होंने सुझाव दिया कि अगर संविधान सभा बनाई जाती है, तो उसमें ऊंची जाति के हिंदू सदस्यों का हिस्सा 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
डॉ. अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन को दिए अपने भाषण ‘कम्युनल डेडलॉक – और इसे हल करने का एक तरीका’ में संविधान सभा की आइडियल बनावट के बारे में अपना विचार बताया।
फिर भी, आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले और उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले बड़े तबकों और समुदायों के बीच हुए समझौते के मुताबिक, और ब्रिटिश सहमति से, 1946 में भारत की संविधान सभा बनाई गई।
क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1935 ने लिमिटेड वोटिंग की शुरुआत की थी, इसलिए 1937 में (और फिर 1946 में ) प्रोविंशियल असेंबली के चुनाव सीमित वोटिंग अधिकारों पर आधारित थे: सिर्फ़ इनकम-टैक्स देने वालों और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को ही “ज़िम्मेदार नागरिक” माना जाता था। 17% से भी कम भारतीयों को वोट देने का अधिकार था; उनमें से लगभग 95% अपर क्लास और अपर कास्ट से थे। यह इलेक्टोरल कॉलेज का सोशियो-इकोनॉमिक और जातिगत बैकग्राउंड था।
इन प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर ने फिर संविधान सभा के लिए 292 सदस्य चुने। और 93 सदस्य रियासतों द्वारा नॉमिनेट किए गए थे।
बंटवारे के बाद, मुस्लिम लीग के सदस्य हट गए, और असेंबली में आखिरकार 299 सदस्य रह गए—229 लिमिटेड वोटिंग से चुने गए और 70 रियासतों द्वारा नॉमिनेट किए गए।
दबे-कुचले लोगों का रिप्रेजेंटेशन कितना था ?
डॉ. अंबेडकर की पूरी ज़िंदगी की लड़ाई सिर्फ़ दलितों और दबे-कुचले लोगों के लिए नंबरों में रिप्रेजेंटेशन पक्का करने के लिए नहीं थी, बल्कि असल रिप्रेजेंटेशन पक्का करने के लिए थी—उनके असली हितों का रिप्रेजेंटेशन। वह जानते थे कि दलित रिप्रेजेंटेटिव दलितों की उम्मीदों को तभी दिखा सकते हैं, जब उन्हें ऊँची जाति के हिंदुओं के दबदबे से अलग चुना जाए।
इसलिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस (1929–32) के दौरान, उन्होंने दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट की मांग की। अंग्रेज मान गए, लेकिन गांधी के अनशन और उसके नतीजे में हुए पूना पैक्ट ने दलितों को हिंदू इलेक्टोरल एरिया में रिज़र्व सीटों पर मजबूर कर दिया।
1937 और 1946 के चुनावों में, रिज़र्व चुनाव क्षेत्रों में दो-स्टेज का प्रोसेस अपनाया गया। पहले राउंड में, सिर्फ़ दलित वोटरों ने चार दलित कैंडिडेट चुने। दूसरे राउंड में, चुनाव क्षेत्र के सभी वोटरों (गैर-दलितों सहित) ने उन चार में से एक को चुना।
डॉ. अंबेडकर की डिटेल्ड स्टडीज़ से एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। जो दलित कैंडिडेट सिर्फ़ दलितों के राउंड में पहले नंबर पर आता था, वह अक्सर जनरल राउंड में सबसे आखिर में आता था और ज़्यादा गैर-दलित वोटों की वजह से हार जाता था।
इस स्ट्रक्चरल कमी को ठीक करने के लिए, अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कड़ा संघर्ष किया। सात बड़ी सबकमेटियों में से, वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता वाली माइनॉरिटीज़ कमेटी ने इस मुद्दे को देखा।
डॉ. अंबेडकर ने प्रस्ताव दिया कि रिज़र्व्ड चुनाव क्षेत्र में जीतने वाले दलित उम्मीदवार को कम से कम 50% दलित वोट मिलने चाहिए, ताकि ऊंची जाति के बहुमत पर निर्भरता के बजाय दलितों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। लेकिन 31 में से 28 सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और यह फेल हो गया।
डॉ. अंबेडकर की गैर-मौजूदगी में, एक सदस्य, नागप्पा ने एक हल्का विकल्प प्रस्तावित किया। एक जनरल (नॉन-रिज़र्व्ड) चुनाव क्षेत्र में, जीतने वाले गैर-दलित उम्मीदवार को कम से कम 35% दलित वोट मिलने चाहिए।
पटेल ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी, और प्रस्ताव को दलितों द्वारा गांधी के प्रति “एहसान फरामोशी” का काम बताया। प्रस्ताव और भी बड़े बहुमत से खारिज हो गया।
आज, हम इसके नतीजे देख रहे हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खुद खोखली और खराब हो गई है – यह हमारे मौजूदा संकट के मूल कारणों में से एक है, जिसमें दलितों का सही प्रतिनिधित्व स्ट्रक्चरल रूप से कमज़ोर बना हुआ है।
विरोधाभासों का दौर
1947 में लिखे अपने दूसरे संवैधानिक प्रस्ताव, ‘स्टेट एंड माइनॉरिटीज़’ में, जिसे उन्होंने संविधान सभा के सामने एक मेमोरेंडम के तौर पर पेश किया था, डॉ. अंबेडकर बताते हैं कि आज़ादी, बराबरी और भाईचारा एक साथ तीन चीज़ें हैं; कोई भी एक के बिना नहीं रह सकता। वह चाहते थे कि हमारा संविधान भी इन तीनों को एक साथ पूरा करे।
उन्होंने तर्क दिया कि बराबरी के बिना आज़ादी, सिर्फ़ खास अधिकार वाले लोगों के लिए ही आज़ादी बन जाती है। अंबेडकर ने साफ़ तौर पर पहचाना कि तब तक मौजूद सभी डेमोक्रेसी ने सिर्फ़ आज़ादी दी थी, बराबरी नहीं। इसलिए, वह चाहते थे कि भारतीय संविधान कुछ और करे और बराबरी को एक बुनियादी अधिकार बनाए।
इस वजह से, उन्होंने तर्क दिया कि देश की दौलत का नेशनलाइज़ेशन होना चाहिए। उन्होंने एक बदलाव लाने वाला प्रोग्राम प्रस्तावित किया: ज़मीन का नेशनलाइज़ेशन करना, कोऑपरेटिव खेती को ज़रूरी बनाना, और इस तरह गरीबों के पसीने से बनी जाति और वर्ग की दीवारें गिराना। राजनीतिक क्षेत्र में, उन्होंने एक और बड़ा कदम सुझाया: किसी भी बहुसंख्यक समुदाय को सरकार या विधानसभाओं में 40% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए।
लेकिन 1950 में जो संविधान लागू हुआ, उसमें बराबरी न तो फंडामेंटल राइट बनी, न ही दौलत का नेशनलाइज़ेशन हुआ। इसके बजाय, दौलत के जमाव को रोकने और इज्ज़त की ज़िंदगी के लिए काफ़ी रिसोर्स पक्का करने से जुड़े प्रोविज़न को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट पॉलिसी के तहत रखा गया।
जैसा कि आर्टिकल 37 साफ़ करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सिर्फ़ गाइड करने वाले आइडियल हैं, लागू करने लायक राइट्स नहीं; सरकारों को उन्हें लागू न करने पर कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अंबेडकर के मुख्य विज़न को कमज़ोर कर दिया और इन रेडिकल आइडियाज़ को संविधान में सजावटी प्रिंसिपल्स तक सीमित कर दिया।
रेडिकल डॉ. अंबेडकर को वापस पाने के लिए
फिर भी, 26 जनवरी, 1950 को भारत एक रिपब्लिक बना—एक बहुत बड़ी सिविलाइज़ेशनल छलांग। जो कुछ भी हासिल हुआ, वह अंबेडकर की दी हुई रोशनी और भारत और दुनिया भर में दबे-कुचले लोगों के संघर्षों से पैदा हुई जागृति की वजह से हुआ।
आज, वह कामयाबी भी खतरे में है। हालांकि पॉलिटिकल बराबरी मौजूद है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक असमानताएं और बढ़ी हैं। ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था, जो सोशल असमानता को और गहरा करती है, और कैपिटलिज़्म, जिसने इकोनॉमिक असमानता को बढ़ाया है, पिछले 75 सालों में, खासकर मोदी के तानाशाही राज के आठ सालों में, काफी मज़बूत हुए हैं।
हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ने सोशल और इकोनॉमिक बराबरी बनाने को ज़रूरी नहीं बनाया। इस बारे में अंबेडकर के विज़न को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने खारिज कर दिया था। इसलिए, उन्हीं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके, ब्राह्मणिज़्म और कैपिटल ने खुद को मज़बूत किया है और आज एक फ़ासिस्ट रूप ले लिया है।
कहावत है कि संविधान के अंदर जो अंबेडकर हैं, उन पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूंजीपतियों और हिंदुत्व ब्राह्मणवादियों की मिली-जुली ताकतों का जानलेवा हमला हो रहा है। दूसरी तरफ, जो लोग डॉ. अंबेडकर को सिर्फ कहने के लिए अपनाते हैं—जैसे धृतराष्ट्र ने आंख मूंदकर गले लगाया था—वे उनके सच्चे मानने वाले होने का दावा करते हैं, जबकि उनके आदर्शों को कम आंकते हैं।
दोनों ताकतें डॉ. अंबेडकर के विजन को खत्म करना चाहती हैं। इसके लिए, वे संविधान पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला करती हैं।
आज के संदर्भ में, जब तक संविधान से बाहर रखे गए डॉ. अंबेडकर को इसमें नहीं लाया जाता, तब तक संविधान के अंदर के डॉ. अंबेडकर को भी नहीं बचाया जा सकता।








